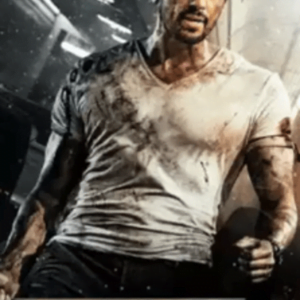Bastar The Naxal Story Movie Review Bastar of Chhattisgarh and…
add comment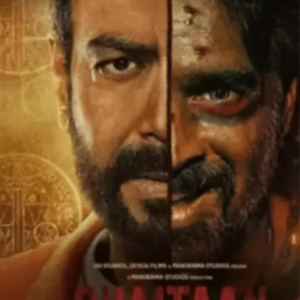
Shaitaan Movie Review Black magic, witchcraft, captures, ASURI powers, all…
add comment
Operation Valentine Movie Review About five years, there was a…
add comment
Laapataa Ladies Movie review The problems of women and many…
add comment
Article 370’ movie review For some time, Bollywood’s tendency towards…
add comment